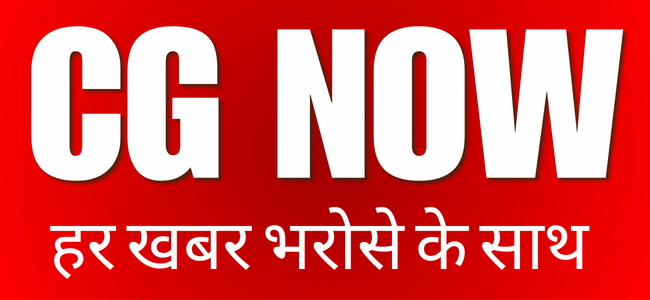Retirement Planning: रिटायरमेंट प्लानिंग पहले आसान हुआ करती थी. 90 के दशक में इसका फॉर्मूला सीधा था – थोड़ी-थोड़ी बचत, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा, अगर हो सके तो एक-दो नए घर, और भरोसा कि पेंशन या बच्चे बुढ़ापे में सहारा देंगे. उस दौर में ज्यादातर परिवार इसी रास्ते पर चलते थे. लेकिन आज ये पुराने ‘गोल्डन रूल्स’ उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं.
BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी का सुनहरा मौका, जल्द करें आवेदन; जानें पूरी डिटेल
मिस्टर शर्मा की मिसाल लीजिए. 58 साल की उम्र में उन्होंने ठीक वही प्लानिंग की, जो 90 के दशक में आईडियल मानी जाती थी. दो मकान खरीदे, ज्यादातर बचत फिक्स्ड डिपॉजिट में डाली और भरोसा रखा कि जरूरत पड़ी तो विदेश में नौकरी कर रहे बेटे का सहारा मिलेगा. लेकिन हकीकत अलग निकली. महंगे इलाज के बिल आने लगे, किराए से उतनी आमदनी नहीं हो पाई कि खर्च पूरे हो सकें और तब जाकर उन्हें समझ आया कि ये रणनीतियां अब वक्त के साथ पुरानी पड़ चुकी हैं.
असलियत ये है कि आज महंगाई, लंबी उम्र, बढ़ते हेल्थकेयर खर्च और फिक्स्ड इनकम पर घटते रिटर्न ने पूरा खेल बदल दिया है. जो प्लानिंग आपके माता-पिता के लिए काम कर गई, वही अगर आप आंख मूंदकर अपनाएंगे तो आपके रिटायरमेंट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. इसलिए सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि पुराने नियमों को आंख बंद करके न अपनाएं – जरूरत पड़ने पर उन्हें भूलना ही पड़ेगा.
आइए अब जानते हैं वे 7 लोकप्रिय रिटायरमेंट रणनीतियां, जो आज के दौर में काम नहीं करतीं और उनकी जगह आपको क्या करना चाहिए…
PGCIL Recruitment 2025: 1500+ इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया
1. सिर्फ FD पर भरोसा करना
90 के दशक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) रिटायरमेंट की सबसे भरोसेमंद रणनीति मानी जाती थी. उस वक्त एफडी पर 12–14% तक ब्याज मिलता था. लोग सिर्फ ब्याज से आराम से घर चला लेते थे और मूल रकम (प्रिंसिपल) को हाथ भी नहीं लगाना पड़ता था. महंगाई कम थी, जरूरतें साधारण थीं, इसलिए एफडी को सुरक्षित और स्थिर आय का पक्का जरिया माना जाता था. यही वजह थी कि ज्यादातर रिटायर लोगों की प्लानिंग सिर्फ एफडी पर टिकी रहती थी.
आज तस्वीर बदल चुकी है. एफडी रेट अब 6–7% पर आ गए हैं, जो कई बार महंगाई से भी कम होते हैं. इसका मतलब यह है कि आपके खर्च हर साल बढ़ते जाएंगे लेकिन आपकी एफडी से मिलने वाली आय उस गति से नहीं बढ़ेगी. धीरे-धीरे आपकी खरीदने की क्षमता घटती जाएगी और आप चाहकर भी अपनी जीवनशैली को बरकरार नहीं रख पाएंगे. यह नुकसान धीरे-धीरे होता है और समय रहते पकड़ में नहीं आता.
तो करना क्या चाहिए? एफडी को पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का अकेला सहारा बनाना गलत है. एफडी को अब “स्टेबलाइजर” की तरह इस्तेमाल करें, न कि मुख्य इंजन की तरह. यानी अपने पोर्टफोलियो में इसका कुछ हिस्सा रखें, लेकिन साथ ही इक्विटी में निवेश करें ताकि लंबे समय तक अच्छी ग्रोथ मिल सके. डेट इंस्ट्रूमेंट्स से स्थिरता पाएं और थोड़े लिक्विड फंड्स हमेशा इमरजेंसी के लिए रखें. असली ध्यान उस निवेश पर होना चाहिए जो महंगाई से तेजी से आगे निकले और आपके अगले 25–30 साल की जिंदगी को आरामदायक बनाए रखे.
2. पेंशन के भरोसे रहना
90 के दशक में नौकरीपेशा लोगों के लिए पेंशन सबसे बड़ी सुरक्षा हुआ करती थी. सरकारी और बड़ी प्राइवेट कंपनियों में यह गारंटी रहती थी कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने तय रकम मिलती रहेगी. यह भरोसा लोगों को सुकून देता था कि बुढ़ापे की जिम्मेदारी उनके नियोक्ता उठाएंगे.
लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. प्राइवेट सेक्टर में पेंशन लगभग खत्म हो गई है और अब केवल EPF जैसी योजनाओं तक ही सीमित रह गई है. नियोक्ता अब आपकी पूरी रिटायरमेंट जिम्मेदारी नहीं उठाते. ऐसे में यह मान लेना कि नौकरी के बाद पेंशन ही आपको सहारा देगी, एक बड़ी भूल साबित हो सकती है.
इसलिए अब जरूरी है कि आप खुद अपना रिटायरमेंट सिक्योरिटी नेट बनाएं. EPF में नियमित योगदान करें, NPS और म्यूचुअल फंड जैसे विकल्पों में निवेश करें और अपने रिटायरमेंट फंड पर लगातार नजर रखें. मानकर चलें कि आपको बाहर से कोई मदद नहीं मिलेगी, और उसी हिसाब से ऐसी प्लानिंग करें जिससे आपकी जीवनशैली रिटायरमेंट के बाद भी बनी रहे.
3. किराए पर निर्भर रहना
90 के दशक में लोग मानते थे कि रिटायरमेंट के लिए सबसे बेहतर रास्ता प्रॉपर्टी खरीदना है. उस समय किराए से होने वाली आमदनी महंगाई से तेज बढ़ती थी और रियल एस्टेट के दाम भी लगातार ऊपर जाते थे. इसलिए कई परिवारों ने दूसरा या तीसरा घर लिया ताकि रिटायरमेंट के बाद किराए से नियमित कमाई होती रहे.
लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है. बड़े शहरों में रेंटल यील्ड (किराए से रिटर्न) बहुत कम हो गया है. ऊपर से रख-रखाव, टैक्स और खाली मकान की दिक्कतें भी हैं. सबसे बड़ी बात यह कि प्रॉपर्टी “लिक्विड” नहीं होती, यानी अचानक जरूरत पड़ने पर आसानी से नकद में बदल पाना मुश्किल है. ऐसे में अगर सिर्फ़ प्रॉपर्टी पर निर्भर रहें तो रिटायरमेंट में मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
बेहतर यही है कि प्रॉपर्टी को घर या लंबी अवधि की संपत्ति मानें, न कि मुख्य कमाई का जरिया. इसे अपने रिटायरमेंट प्लान का सपोर्ट सिस्टम बनाएँ, जबकि असली भरोसा म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एन्युटी और दूसरे लिक्विड असेट्स पर करें.
4. बच्चों के भरोसे रहना
90 के दशक में रिटायरमेंट की सोच काफी अलग थी. उस समय बड़े संयुक्त परिवार आम थे और यह मान लिया जाता था कि बच्चे उम्रदराज मां-बाप की जिम्मेदारी उठाएंगे. इसी भरोसे कई लोग आक्रामक तरीके से बचत नहीं करते थे. उन्हें लगता था कि भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का सहारा बच्चों से मिल जाएगा.
लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. परिवार छोटे हो गए हैं, बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए शहरों और विदेशों में रहते हैं और उनकी अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं. ऐसे में केवल बच्चों पर निर्भर रहना कई बार निराशा और असुरक्षा पैदा कर सकता है.
बेहतर यही है कि खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें. रिटायरमेंट के लिए मजबूत फंड तैयार करें—म्यूचुअल फंड, NPS, EPF में निवेश करें और हेल्थ इंश्योरेंस को मजबूत रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी में सहारा मिल सके. बच्चों की मदद को बोनस समझें, न कि अधिकार. असली सम्मान, सुरक्षा और सुकून तब ही मिलेगा जब बुढ़ापे में आपकी आर्थिक कमान आपके अपने हाथों में होगी.
Job के साथ गलती से भी मत कर लेना इस सब्जेक्ट की Online पढ़ाई, डिग्री को नहीं माना जाएगा वैध
5. मेडिकल खर्चों को हल्के में लेना
90 के दशक में: उस समय हेल्थकेयर खर्च बहुत मामूली थे. ज्यादातर लोग सरकारी अस्पतालों या क्लीनिक में इलाज करा लेते थे, इसलिए मेडिकल खर्चों को लेकर बचत का कोई खास दबाव नहीं था. औसत उम्र भी कम थी, इस वजह से बुजुर्गों को सेहत पर बड़ा फंड बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी.
आज की हकीकत: मेडिकल खर्च अब आसमान छू रहे हैं और हर साल 12-14% तक बढ़ रहे हैं. ऐसे में बिना प्लानिंग के अगर कोई बड़ा इलाज कराना पड़े तो आपकी पूरी रिटायरमेंट बचत खत्म हो सकती है. बिना तैयारी के यह जोखिम आपकी आर्थिक सुरक्षा और जीवनशैली दोनों को नुकसान पहुँचा सकता है.
क्या करें: सेहत से जुड़े खर्चों को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का अहम हिस्सा मानें. कम उम्र में ही हेल्थ इंश्योरेंस ले लें ताकि प्रीमियम कम रहे. इसके साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग फंड रखें और हर साल अपनी कवरेज की समीक्षा करें. सही समय पर सही प्लानिंग आपको बुढ़ापे में आर्थिक आजादी और सम्मान दोनों दे सकती है.
6. आपकी सोच के परे लंबी होती जिंदगी
90 के दशक की बात अलग थी. उस समय भारत में औसतन जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी (Life Expectancy) सिर्फ 60-62 साल के आसपास थी. लोग रिटायर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल तक ही खर्च उठाने की सोचते थे. थोड़ी-सी बचत भी आराम से काम आ जाती थी. शायद यही वजह थी कि तब रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी जटिल नहीं लगती थी.
लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. आज लोग आसानी से 80-90 साल तक जी रहे हैं. यानी रिटायरमेंट के बाद का सफर 25-30 साल लंबा भी हो सकता है. अगर आप पुरानी सोच के हिसाब से छोटी बचत पर भरोसा करते हैं, तो महंगाई और बढ़ते खर्च आपकी प्लानिंग को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर सकते हैं.
तो समाधान क्या है? मान कर चलिए कि आपकी उम्र लंबी होगी और उसी हिसाब से रिटायरमेंट फंड बनाइए. इक्विटी और NPS जैसे लंबे समय वाले निवेश से ग्रोथ पाएं, साथ ही सुरक्षित विकल्पों – जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स – में भी पैसा रखें. लंबी उम्र के लिए प्लानिंग करना न सिर्फ़ आपके लाइफ़स्टाइल को सुरक्षित रखेगा, बल्कि बुढ़ापे की आर्थिक टेंशन से भी बचाएगा.
7. 60 साल में रिटायरमेंट
1990 के दशक में क्यों काम करता था: पहले लोग आमतौर पर 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते थे. इसके बाद वे पूरी तरह काम नहीं करते थे और अपने जीवन के खर्च के लिए पेंशन, बचत या नियोक्ता की मदद पर निर्भर रहते थे. इसलिए, रिटायरमेंट की योजना सिर्फ उम्र 60 पर ही बनती थी.
आज क्यों काम नहीं करता: आज काम करने का तरीका बदल गया है. कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, कुछ जल्दी रिटायर होते हैं. कुछ पार्ट-टाइम या फ्रीलांस काम करते हैं, तो कुछ 70 की उम्र तक अपने शौक या जुनून के काम में लगे रहते हैं. अगर सिर्फ उम्र 60 पर निर्भर रहकर योजना बनाई जाए, तो हो सकता है आपके पास जो चाहिए वो न हो या आप अपनी संपत्ति बढ़ाने का मौका खो दें.
अब क्या करें: रिटायरमेंट की योजना उम्र पर नहीं, बल्कि अपने जीवनशैली पर बनाएं. तय करें कि आप कब पूरी तरह काम छोड़ना चाहते हैं और फिर उसी हिसाब से बचत, निवेश और पैसे निकालने की रणनीति बनाएं. लचीला (Flexible) प्लान होने से आप आराम से जीवन जी सकते हैं और आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं.
कुल मिलाकर, 1990 के दशक की रिटायरमेंट नियम उस समय के हिसाब से बने थे – बैंक में ज्यादा ब्याज, पेंशन, कम खर्च और कम उम्र तक जीना. आज वही नियम अपनाना आपकी संपत्ति और सुरक्षा को धीरे-धीरे नुकसान पहुँचा सकता है. इसलिए अब रिटायरमेंट के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, अलग-अलग जगह निवेश, स्वास्थ्य की तैयारी और लचीले लक्ष्य जरूरी हैं. पुरानी सलाह को भूलकर ऐसा प्लान बनाएं जो आपको दशकों तक शांति, सम्मान और आरामदायक जीवन दे सके.